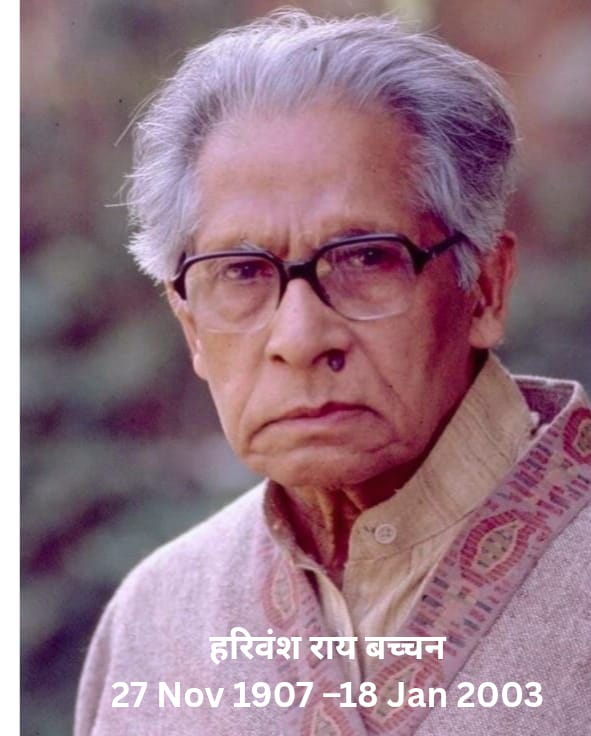जैसे ही आचार संहिता की घोषणा होती है, नेता मौन साध लेते हैं—मानो तपस्या में लीन साधु हों। पर यह तपस्या सत्ता तक पहुँचने का ‘प्रवेश यज्ञ’ होती है। लेकिन जैसे ही चुनावी बिगुल बजता है, वही मौन माइक पकड़ लेता है और शोर का तीर्थ आरंभ हो जाता है। हर गली में मंच, हर चौक पर माइक, और हर माइक पर एक नया “मसीहा”। देश की जनता के कानों में फिर गूँजती है—वादों की शहनाई।
शहर की दीवारें चुनावी पोस्टरों से भर दी जाती हैं, गलियाँ मंडप-सी सज जाती हैं, और लोकतंत्र की यह सजी-धजी बारात चल पड़ती है—वादों की शहनाई के साथ। अब चुनाव विचारों का नहीं, भावनाओं का बाज़ार है। कहीं धर्म की आँच, कहीं जाति का सेंक, कहीं संवेदनाओं की सौदेबाज़ी। हर नेता जनता की नसों में भावनात्मक इंजेक्शन लगाता है—“हमारे बिना तुम सुरक्षित नहीं”, “हम ही तुम्हारे सच्चे हमदर्द हैं”—और जनता सोच में पड़ जाती है।
सच कहूँ तो वोट अब विचार नहीं, वाइब पर पड़ता है। जितना शोर, उतना समर्थन; जितना नाटक, उतना नैरेटिव। हर पार्टी खुद को “सच्चा उद्धारक” बताती है और विरोधी को “राष्ट्रद्रोही” घोषित करती है। किसी के मंच पर “भारत माता की जय” की लहर होती है, तो किसी के मंच पर “संविधान बचाओ” की पुकार। अब रैलियाँ विचारों का मंच नहीं, मनोरंजन का मैदान बन चुकी हैं। रैलियों में जब कोई नेता मंच पर चढ़ते हैं, तो लगता है मानो कोई पुरस्कार लेने जा रहे हों—पीछे झंडे लहरा रहे होते हैं, आगे कैमरे। भाषणों में शब्द नहीं, शब्द-बाण चल रहे होते हैं—तंज पर तंज, और हर तंज में अनूठा व्यंग्य। मंच पर उनके चेहरे ऐसे चमकते हैं जैसे किसी ब्यूटी पार्लर से राष्ट्रभक्ति पैक लगवा कर आए हों।
वादे भी नए ऑफर की तरह पेश किए जाते हैं। अब नेता जनता के दिल नहीं जीतते, डेटा एनालिटिक्स से वोटर की आदतें पढ़ते हैं। मतलब मतदाता अब सिर्फ मतदाता नहीं, टारगेट ऑडियंस बन चुका है—जिसे “फ्री” शब्द सुनते ही तालियाँ बजाने की आदत पड़ चुकी है। मंच से घोषणाएँ इतनी बार दोहराई जाती हैं कि जनता के कानों में अब बिजली से ज़्यादा “फ्री बिजली” गूँजती है। कभी लगता है मानो रैली नहीं, सरकारी योजना वितरण केंद्र खुला हो—जहाँ घोषणा की डिलीवरी तुरंत, पर लाभ का पता अगले कार्यकाल में मिलता है। जनता अब जान चुकी है—जो वादे हवा में उगते हैं, उसके नतीजे धरती पर नहीं टिकते। फिर भी भीड़ जुटती है, क्योंकि जनता जानती है—चुनाव विकल्प का नहीं, उम्मीद का त्यौहार है।
अब लोकतंत्र की जंग सड़कों से ज़्यादा स्क्रीन पर लड़ी जाती है। व्हाट्सऐप यूनिवर्सिटी में ज्ञान नहीं, प्रचार की डिग्रियाँ मिलती हैं। ट्रोल आर्मी सच्चाई को धक्का मारकर अफ़वाह को सिंहासन पर बैठा देती है। हर पोस्ट के नीचे देशभक्ति के सर्टिफिकेट बाँटे जाते हैं। रील्स की ताल पर नारे लिखे जाते हैं और मीम्स की आग में मुद्दे जल जाते हैं। इसलिए कह सकते हैं कि चुनाव अब विचारों की बहस नहीं—एल्गोरिद्म का खेल है।
चुनाव लोकतंत्र का त्यौहार है—और त्यौहार में बाज़ार हमेशा तैयार रहता है। मंच, माइक, झंडे, बैनर, टोपी, टी-शर्ट, माला, कुर्सियाँ—लोकतंत्र का छोटा उद्योग इन्हीं दिनों सबसे ज़्यादा फलता-फूलता है। विकास के काम तो बाद में होंगे, पर चुनावी खर्चे पहले ही GDP को थोड़ा उत्साहित कर देते हैं। इवेंट मैनेजमेंट से लेकर कैटरिंग तक सबमें रौनक आ जाती है। यह एक ऐसा व्यापार है जहाँ मुनाफ़ा तय है—बस जनता को नतीजे मिलने बाक़ी हैं।
मतदान समाप्त होते ही शहनाई के सुर तो मंद पड़ने लगते हैं,
लेकिन शोर का एक नया अध्याय शुरू होता है —
एग्ज़िट पोल का खेल।
हर चैनल अपनी भविष्यवाणियों की थाली लेकर आ जाता है |कहीं सरकार बन रही होती है,कहीं गिर रही होती है,कहीं वोट प्रतिशत की गणित से ऐसा नाच कराया जाता हैमानो पूरी जनता चुनाव नहीं,किसी नृत्य प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर आई हो।
रात भर स्टूडियो में विश्लेषक भविष्यवाणियों का तानपुरा लेकर बैठते हैं|किसी को “सरकार वापसी” की धुन सुनाई देती है,
किसी को “बदलते जनादेश का महासागर”,और जनता सोचती है —
“यह भविष्यवाणी है या प्रायोजित भविष्य?”
एग्ज़िट पोल की इस आतिशबाज़ी में कुछ लोग मोमबत्ती की लौ की तरह उम्मीदें लिए बैठते हैं,और कुछ अपनी निराशा को टीवी की रिमोट में छुपा लेते हैं।
फिर आता है परिणाम का दिन —
जब लोकतंत्र अपना सबसे गंभीर चेहरा दिखाता है। सुबह से ही गली-कूचों में चाय की दुकानों पर चर्चा की भट्ठी जल उठती है —
“कितने राउंड की गिनती हुई?”,“कौन आगे, कौन पीछे?”,“किसका ‘लहर’ निकला, किसका ‘बहाव’ बैठ गया?”
टीवी स्क्रीन पर हर मिनट बदलते अंक किसी शेयर बाजार की तरह ऊपर-नीचे होते रहते हैं। जो कल तक विरोधी था वह अचानक “जनता का प्रतिनिधि” बन जाता है, और जो खुद को निर्विवाद मानता था |वह परिणाम आते ही लोकतंत्र की मार्जिनल लाइन पर फिसल जाता है। परिणाम घोषित होते ही शहर में पटाखे फूटते हैं, जुलूस निकलते हैं, और शहनाई का एक आख़िरी तेज़ सुर हवा में उठता है। लेकिन रात ढलने तक सब शांत हो जाता है |
जनता धीरे-धीरे टीवी बंद कर देती है, कमरों की रोशनी मंद पड़ने लगती है, और अगली सुबह जब शहर जागता है तो चुनाव पीछे छूट चुका होता है |और जिंदगी फिर सामने खड़ी होती है, अपनी उन्हीं समस्याओं के साथ तब लोकतंत्र अपने असली रूप में लौटता है—खेतों में, जहाँ किसान फसलों की चिंता में डूबा है; सड़कों पर, जहाँ युवा अब भी रोजगार की तलाश में भटकता है; कार्यालयों में, जहाँ बाबू फाइलों में जोड़-तोड़ तलाशते हैं; और बाज़ारों में, जहाँ आम आदमी महँगाई की रसीदें गिनता है। शोर के बाद लौट आई खामोशी में लोकतंत्र थका हुआ साँस लेता है। हवा में अब भी कुछ बचे सुर तैरते हैं—“फ्री बिजली… विकास… रोजगार…” जनता धीरे-धीरे फिर अपनी दिनचर्या में लौट जाती है—थकी हुई, पर उम्मीद से भरी।
प्रश्न रह जाता है कि—क्या वादों की यह शहनाई कभी हक़ीक़त की धुन बजा पाएगी?
✍️ — कुन्दन समदर्शी