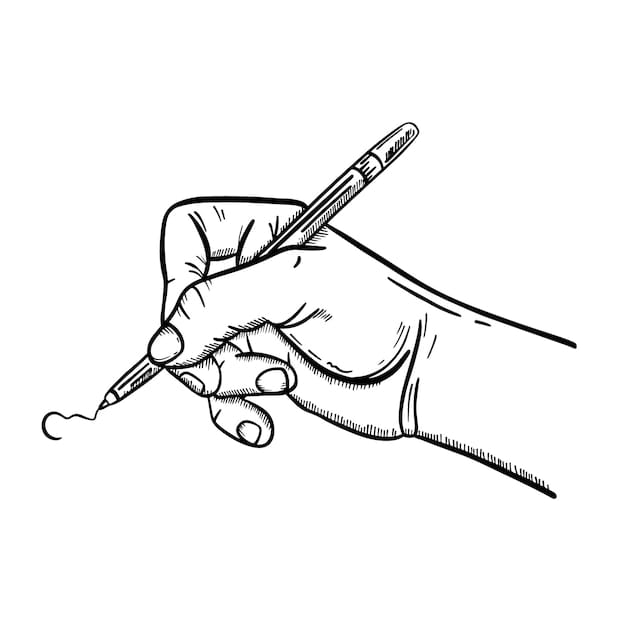✍️-कुन्दन समदर्शीसमकुन्दन समदर्शीदर्शीन् समदर्शी
संघर्षों की धूप देखी है,
ऐ ज़िंदगी…
कितने ज़ख़्मों के निशां अब भी हैं सीने पर।
ये ज़ख़्म…
जो अब
चीखते नहीं,
बस चुपचाप
सीने की तहों में
कुछ गहरी सलवटों-से पड़े हैं,
जिन्हें समय की उँगलियों ने
बस सहलाया – सुलझाया नहीं।
माथे की लकीरें
अब इबारत नहीं रचतीं,
वे बस
अनकहे स्वप्नों के अस्फुट मानचित्र हैं—
जिन्हें वक़्त ने देखा भी,
पर कभी पढ़ा नहीं।
और मैं…
टुकड़ों में बँट चुका हूँ,
फिर भी
हर टुकड़ा मेरी पहचान का
एक मौन प्रत्याशा बनकर
अब तक जीवित है।
शब्द अब थक चुके हैं,
भाव भी चुप हैं,
सिर्फ़ साँसें हैं —
जो समय की चुप्पी में
अपने होने का प्रमाण देती हैं।
मैं अब शिकायत नहीं करता,
बस देखता हूँ—
हर गुज़रते क्षण को
जैसे कोई विस्मृत कथानक
फिर से लिखा जा रहा हो,
बिना किसी पाठक के।
कहीं कुछ शेष नहीं,
सिवाय उस मौन के — जो अब सब कहता है।
अगर ये कविता आपके भीतर कहीं हलचल सी छोड़ गई हो, तो कमेंट कर अपनी अनुभूति ज़रूर साझा करें।
शब्द मौन में उतरते हैं — और शायद वहीं सबसे अधिक बोले जाते हैं।